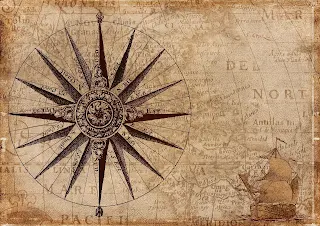
पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल तक उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कृष्णा नदी तक हिंदुस्तान का विशाल भाग किसी एक शक्तिशाली राजा द्वारा केंद्र से शासित हो रहा था। इतने बड़े साम्राज्य में शासन की निश्चित कड़ियां थी, जो शासन को सुचारू रखती थी।
चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शासन प्रबंध को समझने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, वह उस दौर की विद्धान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ चाणक्य द्वारा लिखा “अर्थशास्त्र” और चंद्रगुप्त के शासन में एक यूनानी राजदूत जोकि सेल्यूकस का राजदूत था, मेगस्थनीज। उसने चंद्रगुप्त के साम्राज्य में जो कुछ देखा सुना वह सब कुछ अपनी पुस्तक “इंडिका” में लिखा। मेगास्थनीज के विवरण में चंद्रगुप्त के स्थानीय स्वशासन का काफी विवरण मिलता है।
अध्यन के अंतर्गत चंद्रगुप्त के शासन को समझने के लिए उसे तीन भागों में वितरित किया जा सकता है। केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन।
जो भी हो किंतु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का सर्वोच्च प्रधान राजा होता था, वह केंद्रीय सकती थी, और वह स्वेच्छाचारी भी हो सकता था, और निरंकुश शासन करता था। वह सर्वेसर्वा था।
इस सब में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ज्ञान प्राप्त होता है, कि राजा प्रजा के प्रति ऋणी होता है, और वह प्रजा को सुख शांति दे कर उस ऋण से मुक्त हो सकता है।
केंद्रीय शासन का तात्पर्य है, जो राजधानी से संचालित होता था। सम्राट केंद्रीय शासन का प्रधान था, वही कानून बनाता था, और उनका पालन भी वही करवाता था। कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को दंड भी वही देता था।
सम्राट द्वारा नियुक्त एक मंत्री परिषद अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर सम्राट को परामर्श देती थी। वह सम्राट के विश्वासपात्र होते थे, हालांकि वह केवल वेतनभोगी मंत्री थे, और सम्राट उनकी राय को मानने के लिए बाध्य ना था। दैनिक कार्यों में मंत्री परिषद का कोई भूमिका न थी।
दैनिक कार्यों में परामर्श देने के लिए सम्राट के साथ मंत्रिन् हुआ करते थे। इन्हीं के सहायता से सम्राट शासन संचालित करता था। किंतु सम्राट इनके भी परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं था।
चंद्रगुप्त के काल में शासन को संचालित करने के लिए अनेक विभागों में शासन को बांटा गया था। उस समय में कुल 18 विभाग थे। प्रत्येक विभाग को एक-दो विषय सौंप दिए गए थे। विभाग का अध्यक्ष अमात्य होता था। अमात्य के नीचे आनेक सारे कर्मचारी पदाधिकारी होते थे। वह दैनिक शासन को चलाते थे, और राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे।
अपने साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए चंद्रगुप्त ने पुलिस या आरक्षी विभाग का संगठन किया था। इस विभाग के कर्मचारी “रक्षिन्” कहलाते थे। जनता की रक्षा ही इनका कर्तव्य था।
इसके अतिरिक्त इतने बड़े साम्राज्य में जगह जगह पर हो सकने वाले अपराधों और षड्यंत्र को रोकने के लिए राजा ने गुप्तचर विभाग भी काम में रखा था। वे “संस्थान” गुप्तचर जो कि निश्चित स्थान पर रहकर, और “संचारण” गुप्तचर जो कि घूम घूम कर अपराधियों का पता लगाते थे, संभवत संचारण गुप्तचर साम्राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विचरण कर वहां होने वाले अपराधों और षड्यंत्रों का पता लगाते रहे होंगे। जानकारी है कि, स्त्रियां भी गुप्तचर के कार्यों करती थी। इस प्रकार से सम्राट को अपराधों कुचक्रों और षड्यंत्रों की सूचना अपने साम्राज्य के कोने कोने से प्राप्त हो जाती थी।
अपराधिक मामलों में न्याय व्यवस्था का प्रधान भी स्वयं चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त की सहायता के लिए न्यायधीश हुआ करते थे। वह नगरों तथा जनपदों के लिए अलग-अलग न्यायाधीश होते थे। नगरों के न्यायाधीश “व्यवहारिक” और जनपद के न्यायधीश “राजुक” कहलाते थे। न्यायाधीशों को “धर्मस्थ” के नाम से भी जाना जाता था। प्रत्येक न्यायालय में तीन धर्मस्थ तथा तीन अमात्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करते थे। दीवानी तथा फौजदारी मामले में अलग-अलग न्यायाधीश होते थे। दीवानी के न्यायालय “धर्मस्थीय” तथा फौजदारी न्यायालय “कण्टशोधक” कहलाते थे।
दंड विधान बहुत कठोर था। जुर्माना, अंग-भंग और मृत्यु तक का दंड दिया जाता था। स्ट्रेबो ने लिखा कि यदि कोई झूठी गवाही देता, तो उसका अंग-भंग का दंड दिया जाता, यदि कोई किसी का अंग-भंग कर देता है तो उसका हाथ काट दिया जाता और यदि कोई अपराधी किसी कारीगर का अंग-भंग कर देता तो उसे प्राण दंड दिया जाता था।
सबसे महत्वपूर्ण कि इतना कठोर दंड विधान होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में अधिक अपराध नहीं होते थे।
राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के काल में न्यायालय की बैठक प्रातः काल होती थी, और निर्णय में शीघ्रता होती थी। छोटी अदालतों के फैसलों की अपील बड़ी अदालतों में होती थी। और सम्राट का निर्णय अंतिम निर्णय होता था।
चाणक्य की कथानानुसार राजा प्रजा के प्रति ऋणी है, वह लोग मंगलकारी कार्यों को करने से ही प्रजा के ऋण से मुक्त हो सकता है। अतः चंद्रगुप्त ने अपने काल में यातायात के लिए सड़के बनाई, छायादार वृक्ष राहों में और स्थान स्थान पर कई कुएं तथा धर्मशालाएं बनाई। सिंचाई की समुचित व्यवस्था की, उसके प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने सौराष्ट्र में सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ी झील जिसका नाम सुदर्शन झील हुआ का निर्माण करवाया।
स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की समुचित व्यवस्था की गई थी। “भैष्ज्य गृहों” अर्थात औषधालय की स्थापना करवाई। उसमें चिकित्सकों की व्यवस्था की गई, शिक्षा का समुचित व्यवस्था की गई, छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, शिक्षा का प्रबंध प्रधानमंत्री और पुरोहित की अध्यक्षता में संचालित होता था।
Comments
Post a Comment
Please comment your review.